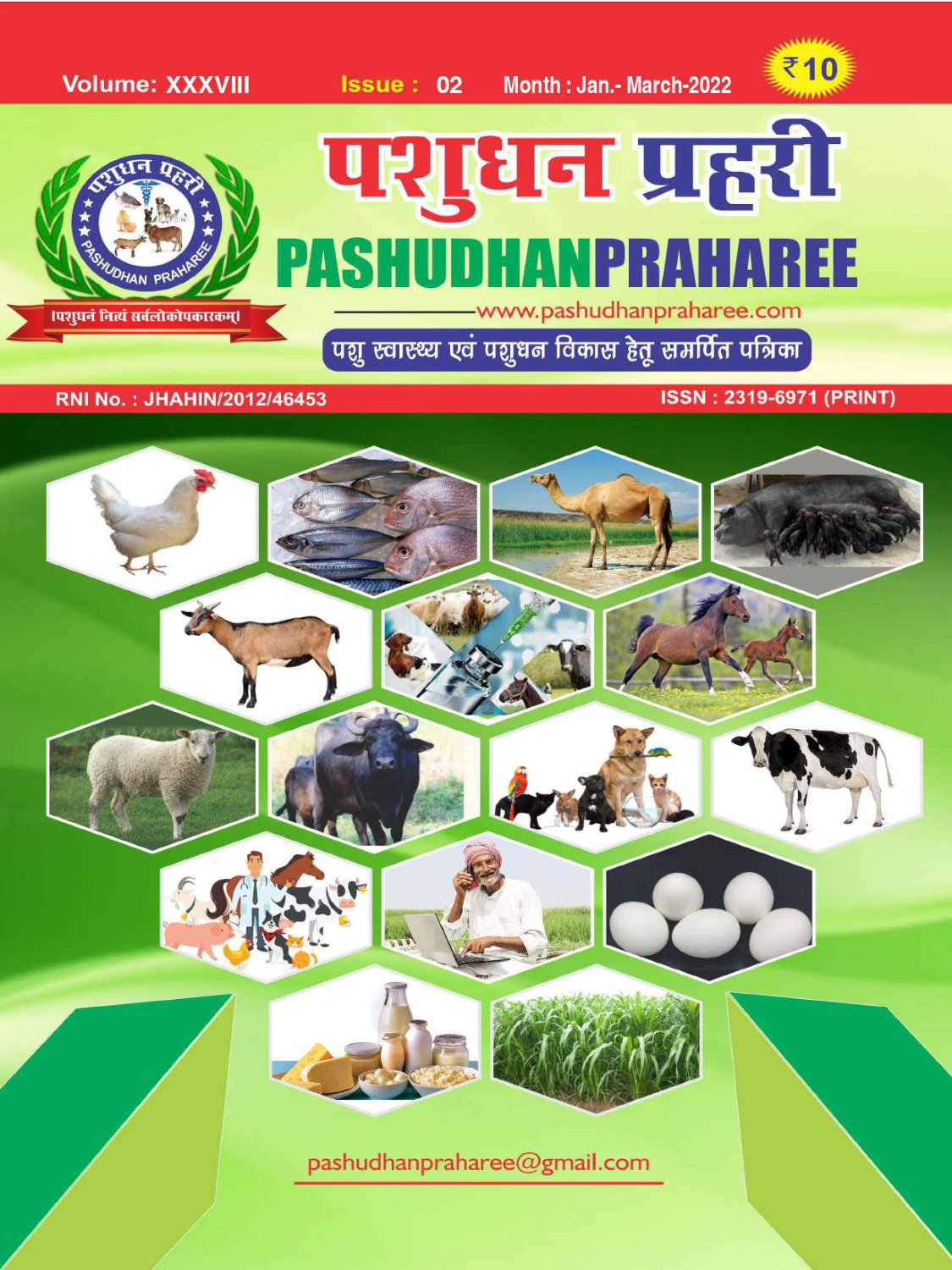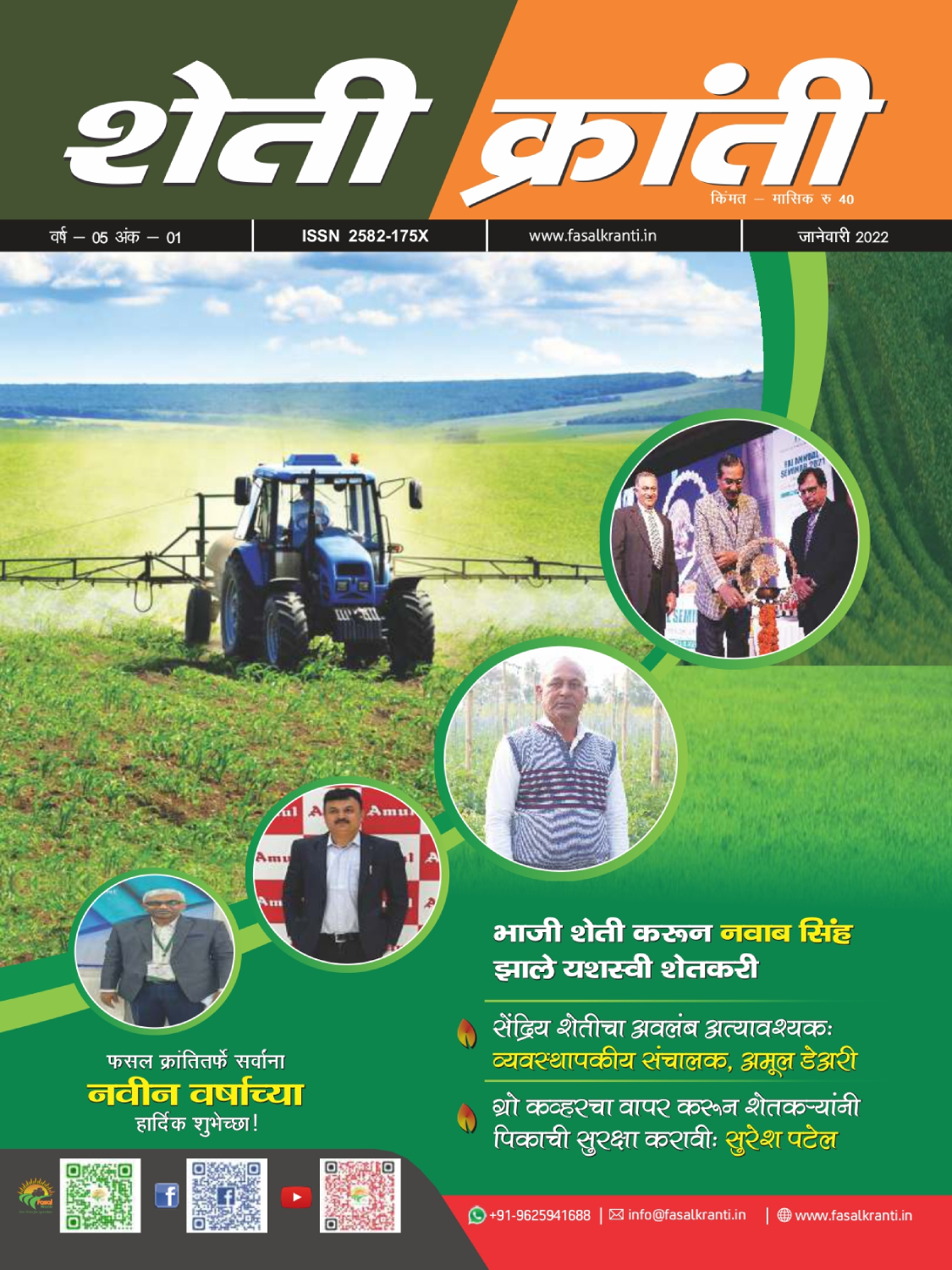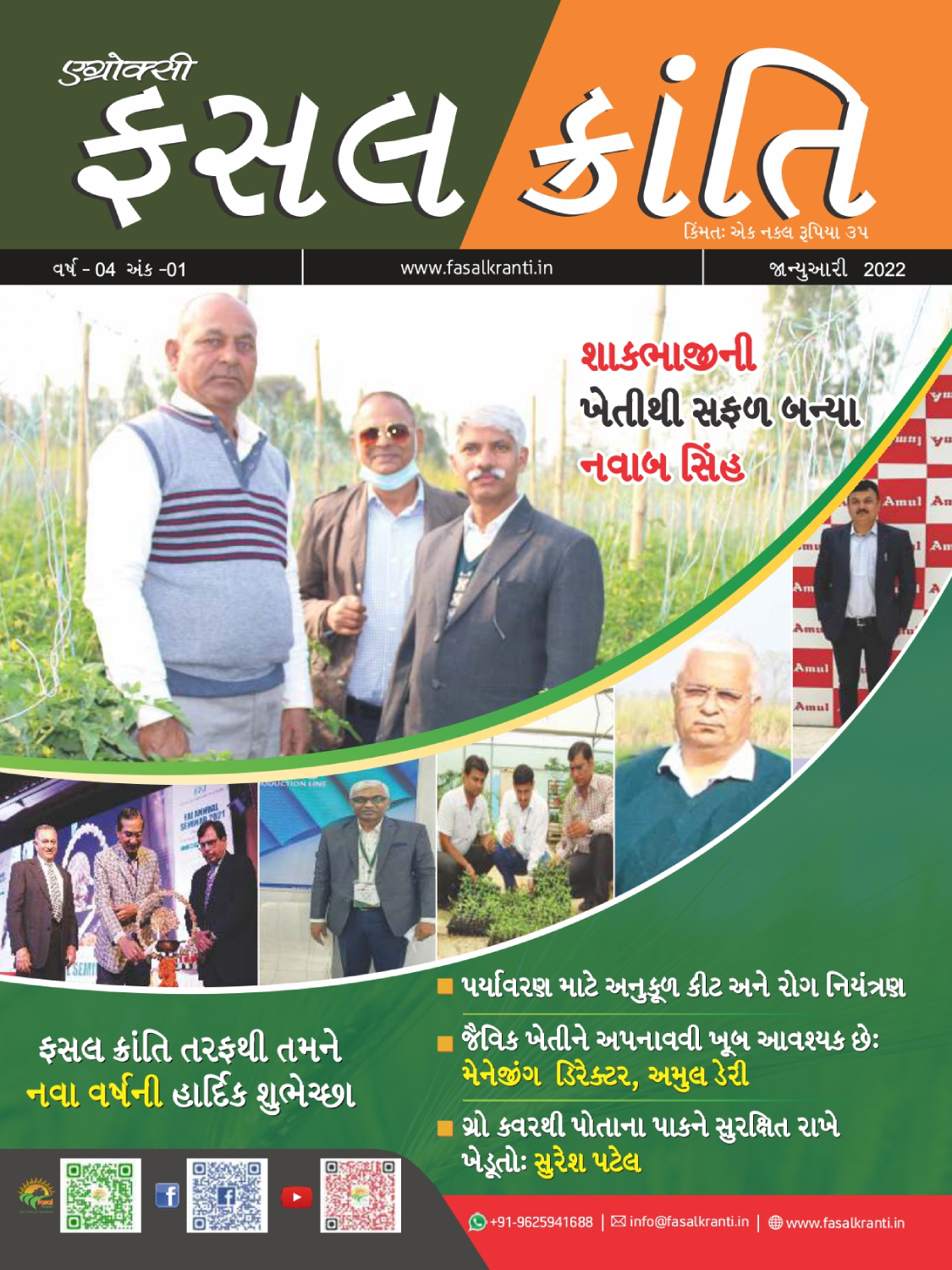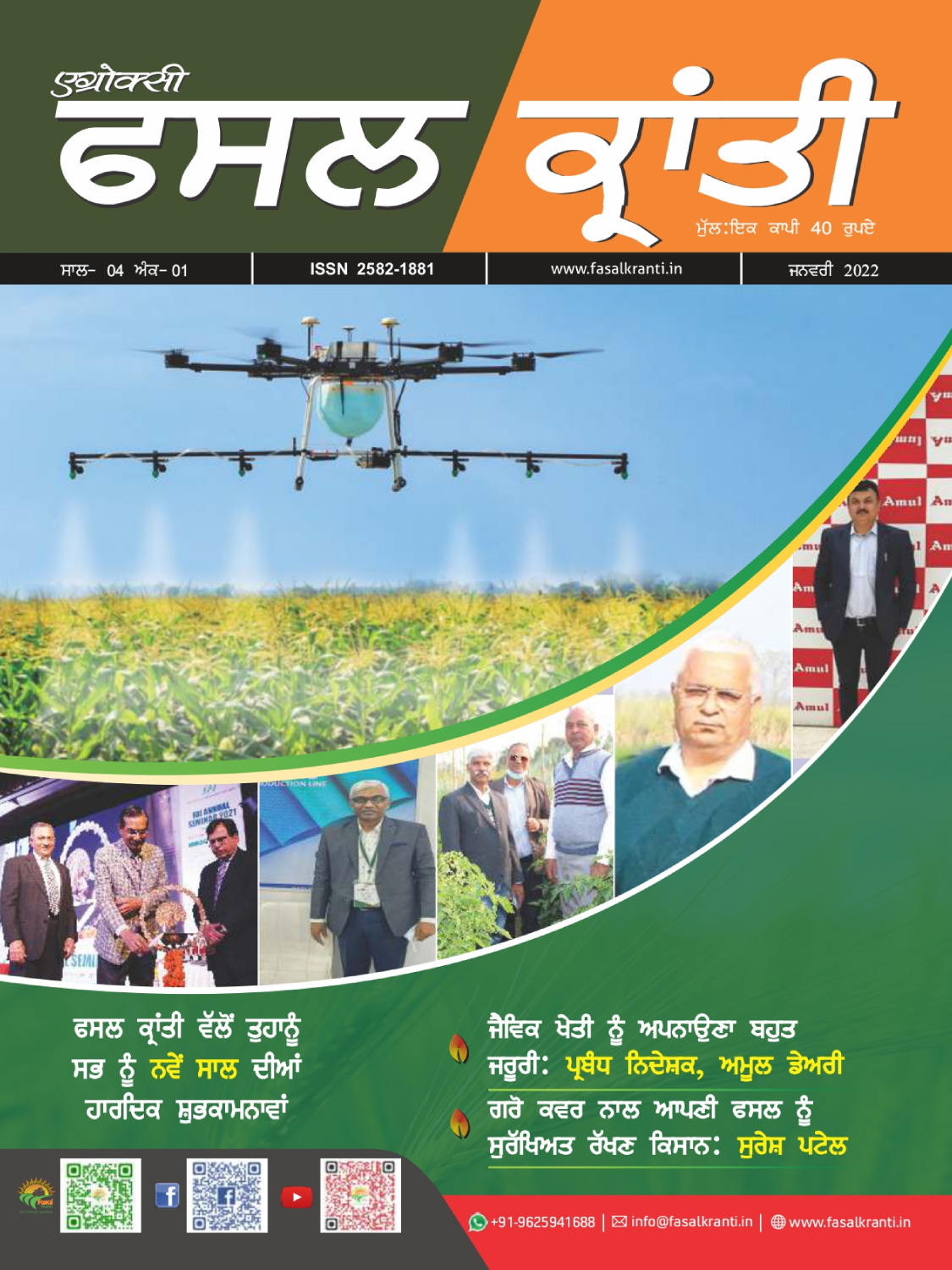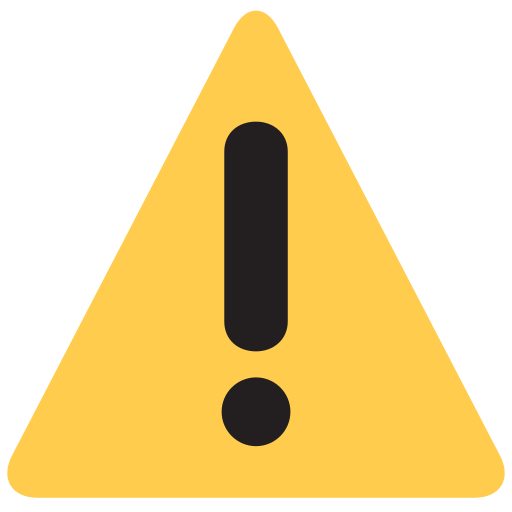विवेकानंद से जुड़ी ये कहानियां किसी की भी सोच बदल सकती हैं


Kisaan Helpline
जो सत्य है, उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। ये बातें किसी साधारण शख्सियत ने नही विवेकानंद ने कही हैं। विवेकानंद एक ऐसा व्यक्तितत्व है, जो हर युवा के लिए एक आदर्श बन सकता है। उनकी कही एक भी बात पर यदि कोई अमल कर ले तो शायद उसे कभी जीवन में असफलता व हार का मुंह ना देखना पड़े। आइए आज जानते है स्वामी विवेकानंद से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक किस्सों को जो किसी के लिए भी प्रेरणा बन कर उसका जीवन बदल सकते हैं।
एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक, एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बन्दूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने ने एक लड़के से बन्दूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिलकुल सही लगा, फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए। सभी बिलकुल सटीक लगे।
ये देख लड़के दंग रह गए और उनसे पुछा - स्वामी जी, भला आप ये कैसे कर लेते हैं ? आपने सारे निशाने बिलकुल सटीक कैसे लगा लिए? स्वामी विवेकनन्द जी बोले असंभव कुछ नहीं है, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो।
स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और सभी लोग उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो अपने साथी छात्रों से कुछ बताते तो सब मंत्रमुग्ध हो कर उन्हें सुनते थे। एक दिन कक्षा में वो कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे, सभी उनकी बातें सुनने में इतने मग्न थे की उन्हें पता ही नहीं चला की कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढऩा शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी।कौन बात कर रहा है? मास्टर जी ने तेज आवाज़ में पूछा। सभी छात्रों ने स्वामी जी और उनके साथ बैठे छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी क्रोधित हो गए।
उन्होंने तुरंत उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबधित प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तब अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से भी वही प्रश्न किया, स्वामी जी तो मानो सब कुछ पहले से ही जानते हों , उन्होंने आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। यह देख मास्टर जी को यकीन हो गया कि स्वामी जी पाठ पर ध्यान दे रहे थे और बाकी छात्र बात-चीत में लगे हुए थे।फिर क्या था।
उन्होंने स्वामी जी को छोड़ सभी को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र एक-एक कर बेच पर खड़े होने लगे, स्वामी जी ने भी यही किया। मास्टर जी बोले - नरेन्द्र तुम बैठ जाओ!नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा क्योंकि वो मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था। स्वामी जी ने आग्रह किया। सभी उनकी सच बोलने की हिम्मत देख बहुत प्रभावित हुए।
एक बार बनारस में स्वामी विवेकनन्द जी मां दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे कि तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनसे प्रसाद छिनने लगे वे उनके नज़दीक आने लगे और डराने भी लगे। स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़ कर भागने लगे। वो बन्दर तो मानो पीछे ही पड़ गए और वे भी उन्हें पीछे पीछे दौड़ाने लगे।
पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहे थे, उन्होनें स्वामी जी को रोका और कहा - रुको! डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। वृद्ध सन्यासी की ये बात सुनकर स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों के तरफ बढऩे लगे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनके ऐसा करते ही सभी बन्दर तुरंत भाग गए। उन्होनें वृद्ध सन्यासी को इस सलाह के लिए बहुत धन्यवाद किया।
इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में इसका जिक्र भी किया और कहा - यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो, तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। वाकई, यदि हम भी अपने जीवन में आये समस्याओं का सामना करें और उससे भागें नहीं तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जायेगा!
स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, मां की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है? स्वामी जी मुस्कराए, उस व्यक्ति से बोले, पांच सेर वजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बाँध लो और चौबीस घंटे बाद मेरे पास आओ तो मई तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा।
स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिनभर वो अपना कम करता रहा, किन्तु हर छण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते-होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए असह्य हो उठा। थका मांदा वह स्वामी जी के पास पंहुचा और बोला मैं इस पत्थर को अब और अधिक देर तक बांधे नहीं रख सकूंगा।
एक प्रश्न का उत्तर पाने क लिए मै इतनी कड़ी सजा नहीं भुगत सकता स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी नहीं उठाया
गया। मां अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे नौ माह तक ढ़ोती है और ग्रहस्थी का सारा काम करती है। संसार में मां के सिवा कोई इतना धैर्यवान और सहनशील नहीं है। इसलिए माँ से बढ़ कर इस संसार में कोई और नहीं।
एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली मैं आपस शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद बोले क्यों?मुझसे क्यों ?क्या आप जानती नहीं की मैं एक सन्यासी हूं?औरत बोली मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूं और वो वह तब ही संभव होगा। जब आप मुझसे विवाह करेंगे।
विवेकानंद बोले हमारी शादी तो संभव नहीं है, परन्तु हां एक उपाय है। औरत- क्या? विवेकानंद बोले आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं। आज से आप मेरी मां बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा।औरत विवेकानंद के चरणों में गिर गयी औरबोली की आप साक्षात् ईश्वर के रूप है ।इसे कहते है पुरुष और ये होता है पुरुषार्थ एक सच्चा पुरुष सच्चा मर्द वो ही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अन्दर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके।
Relevant News
Smart farming and agriculture app for farmers is an innovative platform that connects farmers and rural communities across the country.
Explore
Important Link
© All Copyright 2024 by Kisaan Helpline