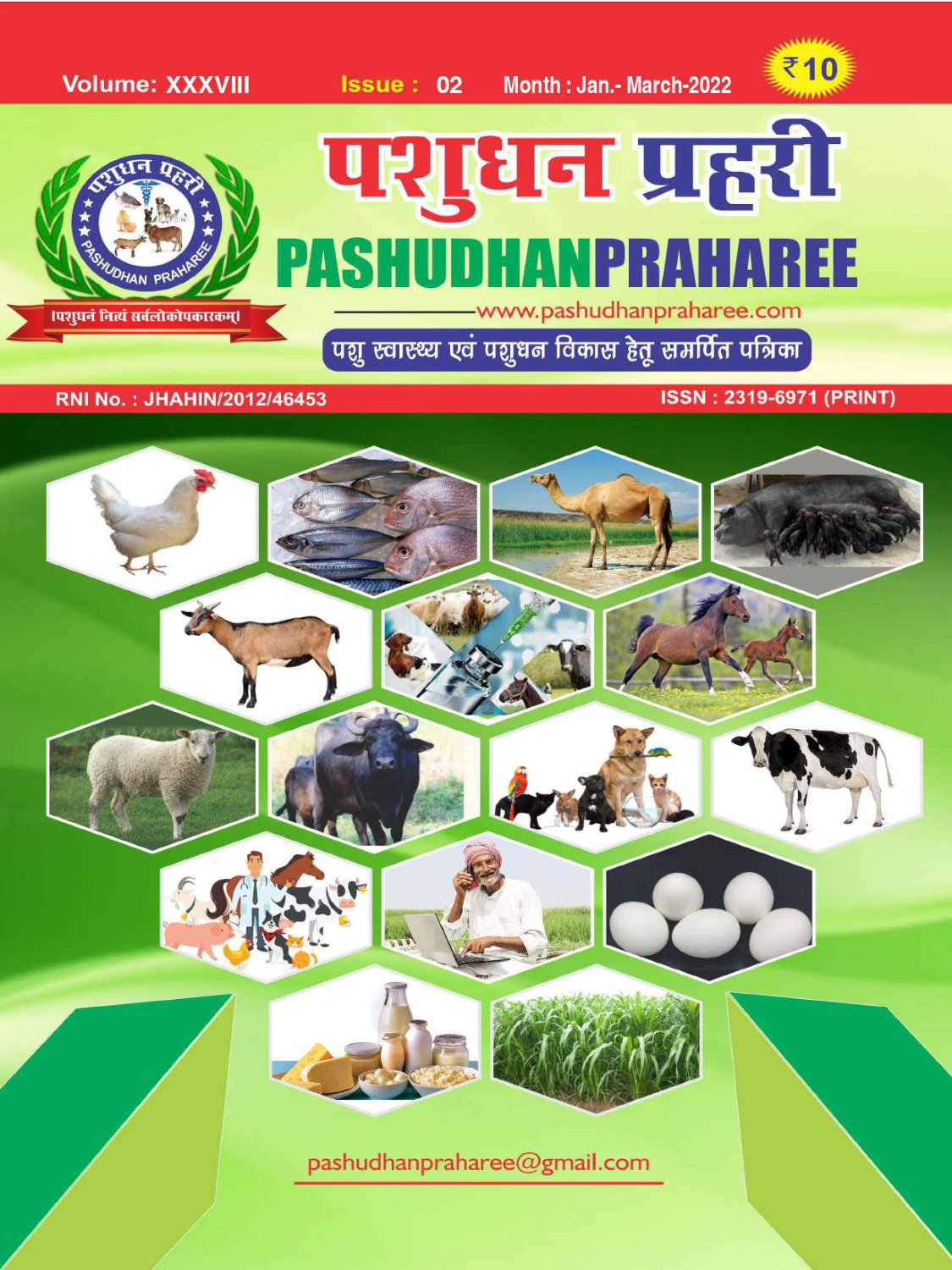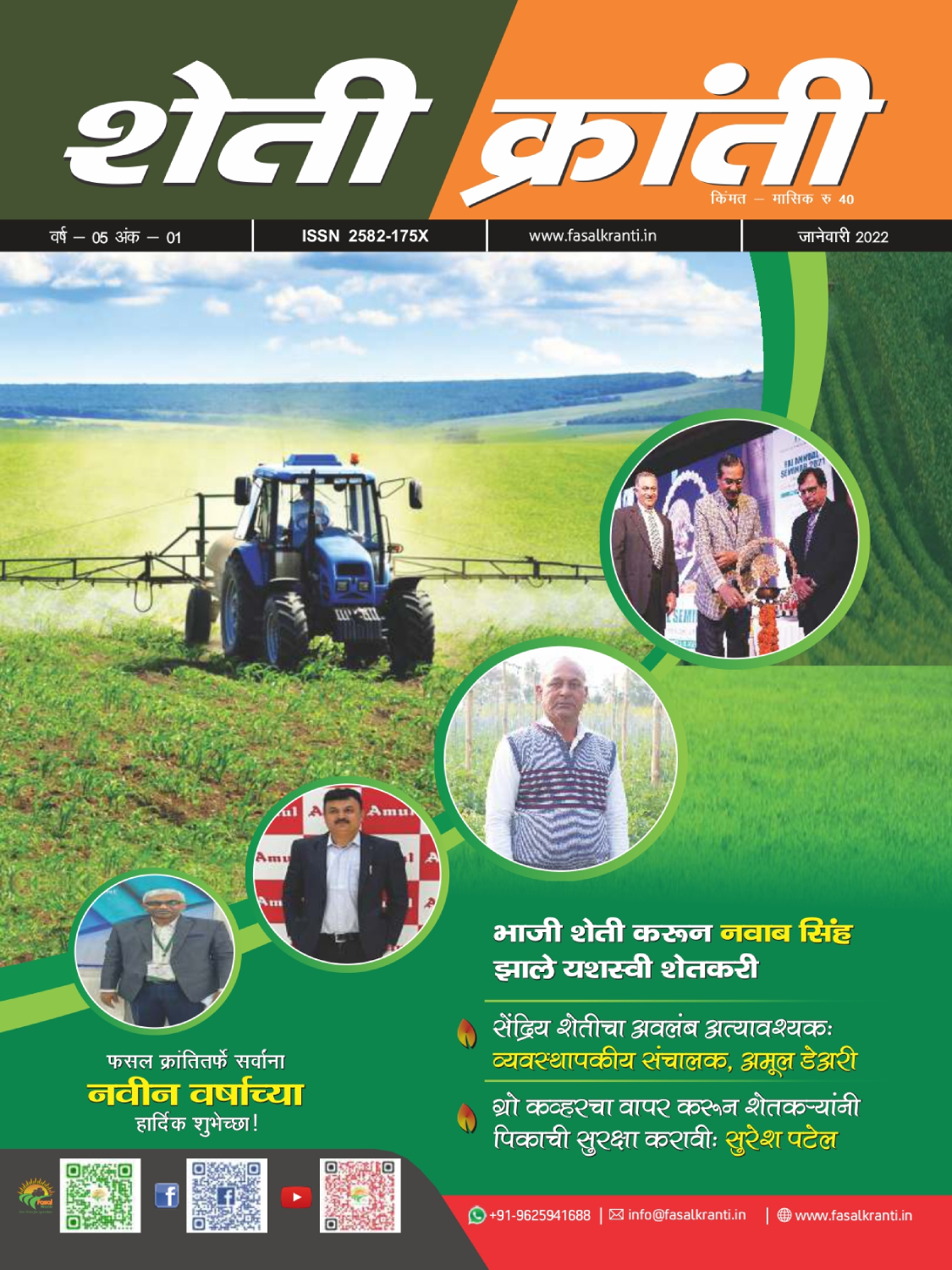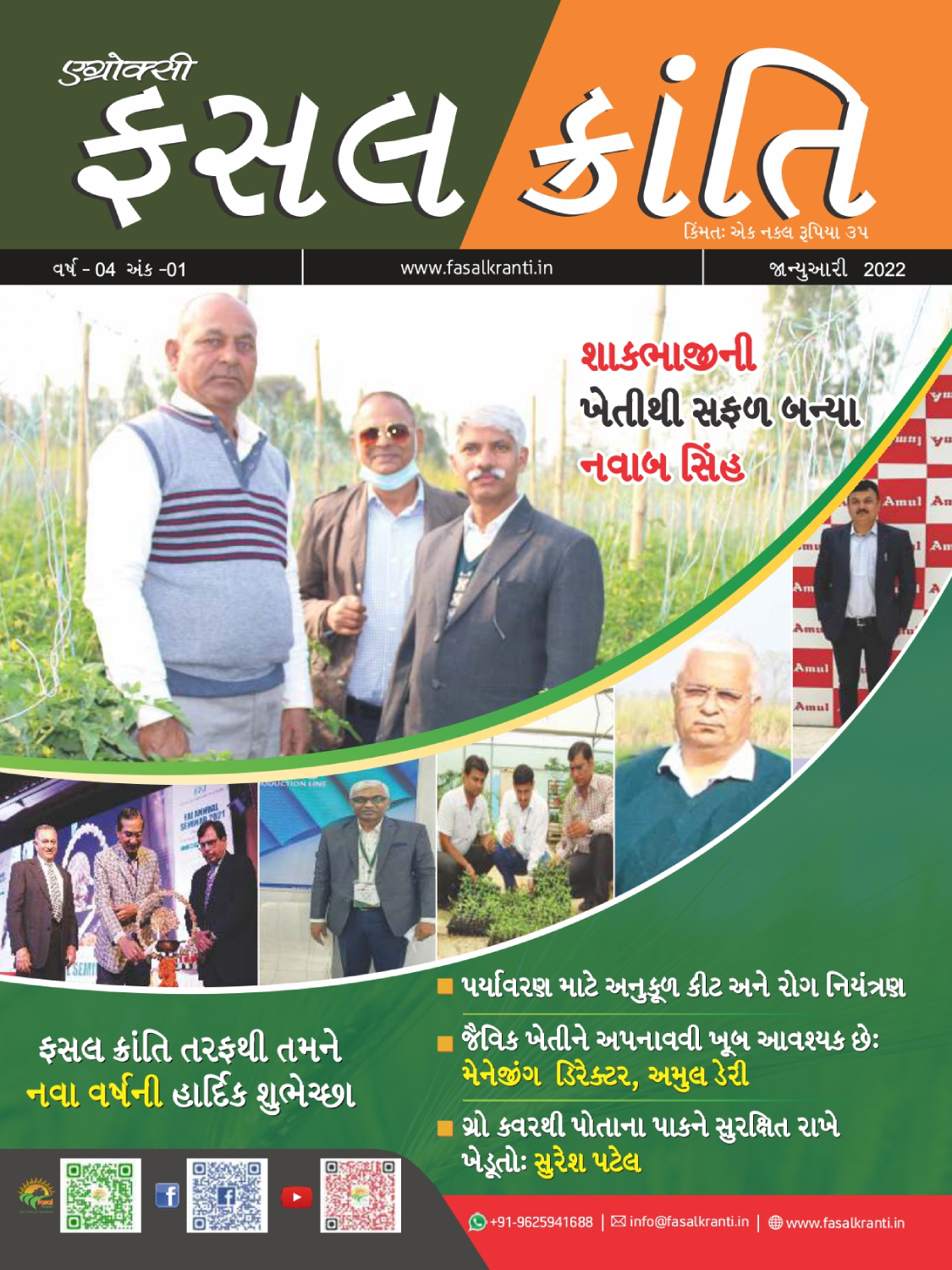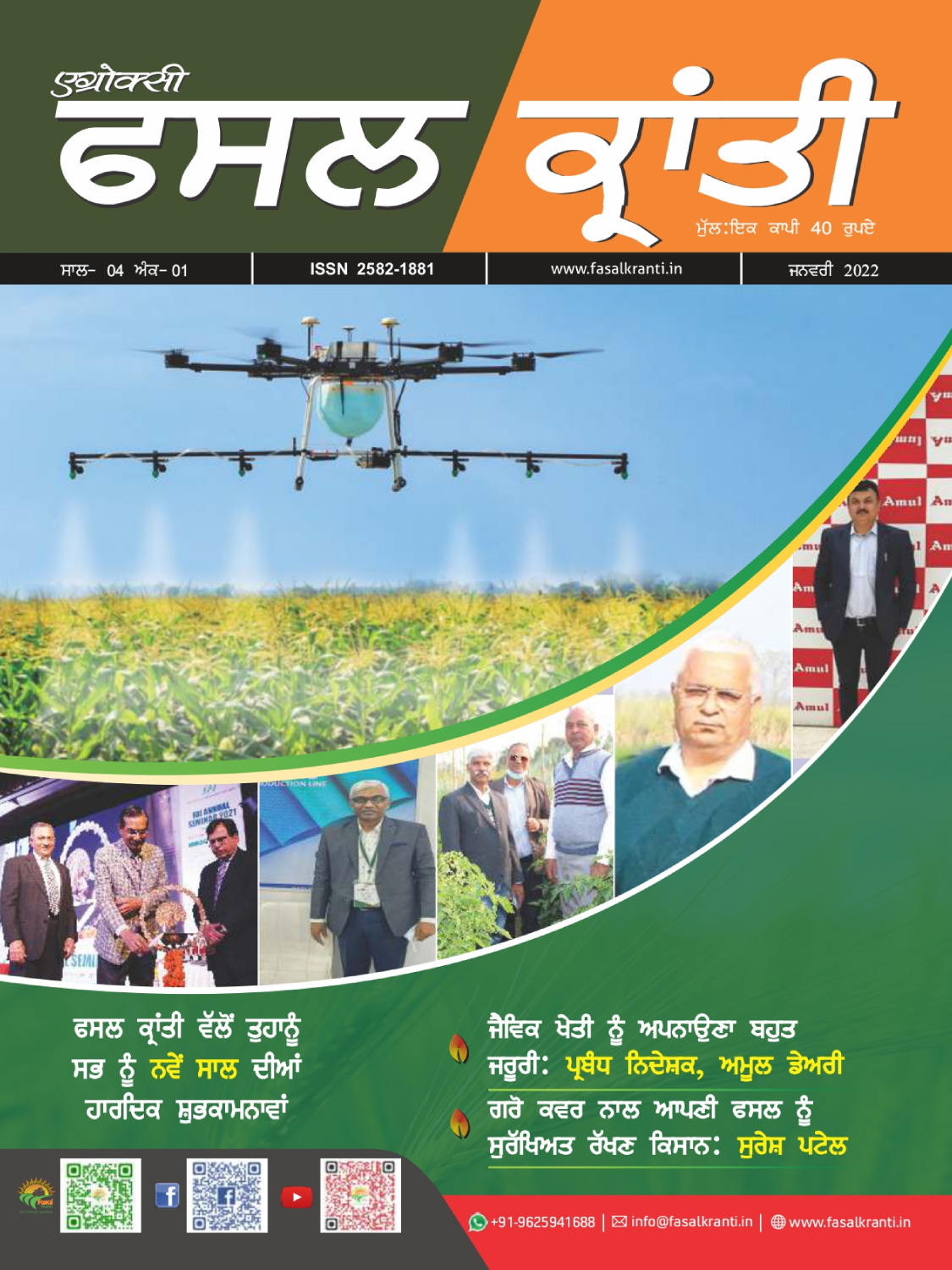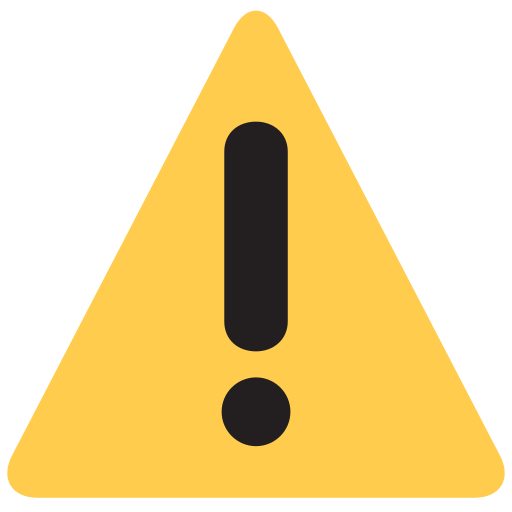अखबार बांटकर करता रहा पढ़ाई, अब टॉपर बना किसान का बेटा


Kisaan Helpline
Scheme
May 18, 2015
धार(इंदौर). हाईस्कूल की परीक्षा में धार जिले के ग्राम सेमल्दा के छात्र शिव कुशवाह ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आठवां स्थान प्राप्त किया है। उसे 96.3 प्रतिशत अंक मिले। शिव के पिता किसान हैं और वे डेढ़ बीघा जमीन पर खेती कर घर चलाते हैं, जबकि मां अल्प शिक्षित। वह खुद भी अखबार बांटकर परिवार में सहयोग करता है। बचे हुए समय में पढ़ाई करता है।
सरकारी हाईस्कूल में पढ़ने वाले शिव ने कभी ट्यूशन का सहारा नहीं लिया। परिणाम आने पर उसने कहा- मुझे यकीन था क्योंकि गुरुओं ने यही बताया कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। प्राचार्य प्रवीण शुरकर ने बताया शिव का पढ़ाई के लिए जुनून देखते ही बनता है। शिव नवोदय विद्यालय में भी चयनित हुआ था लेकिन एक वर्ष बाद ही पढ़ाई छोड़कर आना पड़ा। माता रेखा बाई आठवीं पास हैं, लेकिन पढ़ाई का महत्व जानती हैं, इसलिए पुत्र को पढ़ते समय परेशानी ना हो इसका जरूर ध्यान रखती थी।
Relevant News
Smart farming and agriculture app for farmers is an innovative platform that connects farmers and rural communities across the country.
Explore
Important Link
© All Copyright 2024 by Kisaan Helpline